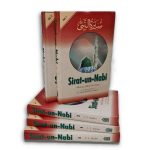तलाक-ए-हसन शरीअत की नज़र से : न्याय, जवाबदेही और नैतिक सुधार
निर्मल कुमार
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 26 नवम्बर 2025 को मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंतर्गत तलाक-ए-हसन की प्रथा की संवैधानिकता और सामाजिक प्रभावों का गहन परीक्षण करते हुए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया । यह वह क्षण था जब देश ने एक बार फिर देखा कि कैसे अदालतें परंपरा, शरीअत और आधुनिक कानून के संगम पर खड़ी होकर समकालीन समाज के लिए संतुलित रास्ता तलाशती हैं।
तलाक-ए-हसन, इस्लामी न्यायविदों के अनुसार, ऐसा तलाक है जिसमें एक निश्चित प्रतीक्षा अवधि और पुनर्मिलन का अवसर निहित रहता है। इसमें पति और पत्नी को अपने वैवाहिक संबंध पर पुनर्विचार करने का समय दिया जाता है। पहली तथा दूसरी बार उच्चारण के बाद विवाह अभी भी पुनर्स्थापित किया जा सकता है, परन्तु तीसरे उच्चारण के बाद यह तलाक अंतिम और अपरिवर्तनीय हो जाता है । इसे तलाक-ए-बिद्दत की तुलना में अधिक विचारशील, मर्यादित और गरिमापूर्ण प्रक्रिया माना गया है, क्योंकि इसमें दम्पत्ति को समय और सम्भावना दी जाती है।
आज के डिजिटल समाज में, जब रिश्ते तेजी से बनते और बिखरते हैं, यह मॉडल न्यायपालिका के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करता है कि व्यक्तिगत कानून केवल धार्मिक आज्ञा नहीं, बल्कि मानवीय संवेदना के आधार पर भी समझे जाने चाहिए। अदालत ने स्पष्ट रूप से यह दर्शाया कि धार्मिक ढाँचे के भीतर भी शालीनता, सुनवाई और महिलाओं की सुरक्षा सर्वोपरि रहनी चाहिए।
न्यायालय का हस्तक्षेप : प्रक्रिया की त्रुटियाँ और पीड़ित पक्ष की असुरक्षा
सुप्रीम कोर्ट ने तलाक-ए-हसन के मामले में हस्तक्षेप इस दृष्टि से भी आवश्यक पाया कि कई मामलों में प्रक्रिया की विसंगतियाँ पीड़ित पक्ष, विशेषतः महिलाओं, को न्याय के लिए उच्चतम अदालत तक जाने को बाध्य कर देती हैं । अदालत का कक्ष एक ऐसे मंच में बदल जाता है जहाँ पुरुष-प्रधान निर्णय-प्रक्रिया उजागर होती है और महिलाओं की आवाज़ अक्सर पीछे छूट जाती है।
मुख्य याचिका में अदालत ने उस पति से कठोर प्रश्न किए जिसने बिना हस्ताक्षर वाले नोटिस के माध्यम से अपने अधिवक्ता से तलाक दिलाने की चेष्टा की। अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि वैवाहिक विघटन की प्रक्रिया में प्रतिनिधि-संप्रेषण (delegation) की अनुमति नहीं दी जा सकती क्योंकि इससे प्रक्रिया की पवित्रता और महिला की गरिमा प्रभावित होती है ।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत का प्रश्न —
“क्या आप अपने वकील को निर्देश दे सकते हैं, पर अपनी पत्नी का सामना करने का साहस नहीं?”
शायद इस मुकदमे की सबसे महत्वपूर्ण पंक्ति बनकर उभरा। अदालत ने पति को निर्देशित किया कि वह अपनी पत्नी हीना और बच्चे के साथ संवाद स्थापित करे, स्वयं निर्णय व्यक्त करे और शरीअत में अपेक्षित जिम्मेदारी निभाए ।
हीना ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि दस्तावेज़-अस्पष्टता के कारण उसके बेटे के स्कूल प्रवेश, पासपोर्ट नवीनीकरण और अभिरक्षा जैसे मुद्दों पर गंभीर अड़चनें उत्पन्न हुईं। अदालत ने तत्परता से राहत प्रदान की और आवश्यक अंतरिम आदेश जारी किए ।
शरिया और संविधान का संगम : समानता, गरिमा और स्वतंत्रता
2017 की प्रसिद्ध शायरा बानो बनाम भारत संघ मामले में तलाक-ए-बिद्दत को अवैधानिक घोषित किया गया था। इसी संदर्भ में न्यायालय ने तलाक-ए-हसन पर गहराई से विचार करते हुए कहा कि यदि तलाक को धार्मिक प्रावधानों के अनुसार क्रियान्वित करना है, तो हर चरण का शुद्ध पालन अनिवार्य है ।
अदालत ने यह भी कहा कि तीसरे पक्ष द्वारा तलाक भेजना न केवल असंवैधानिक है बल्कि महिला-सम्मान, एजेंसी और अधिकारिता को भी नुकसान पहुँचाता है।
सभा-कक्ष में यह बहस केवल तलाक की तकनीकी प्रक्रिया तक सीमित नहीं रही; यह महिलाओं की आवाज़, सुरक्षा, वित्तीय अस्तित्व और पुनर्विवाह-समान अधिकारों की लड़ाई का प्रतीक भी बन गई। जब धार्मिक नियमों का गलत उपयोग होता है, तब स्त्री अक्सर सबसे बड़ा नुकसान झेलती है — आर्थिक, सामाजिक और मानसिक तीनों स्तरों पर। अदालत ने इसी बिंदु पर जोर देते हुए कहा कि इस्लामी सिद्धांत न्याय और करुणा पर आधारित हैं, और यदि प्रक्रिया महिला को असुरक्षित बनाती है, तो उसका सुधार नैतिक दायित्व है।
तलाक-ए-हसन का व्यापक प्रभाव: सुधार, पुनर्मिलन और सामाजिक संदेश
अदालत ने एआईएमपीएलबी तथा जमीयत-उलमा-ए-केरल को भी इस बहस का हिस्सा बनने की अनुमति दी, ताकि इस्लामी विवाह-क़ानूनों पर समग्र दृष्टिकोण स्थापित हो सके । इस्लामी शिक्षाओं में ‘सुलह’ सर्वोत्तम मार्ग मानी जाती है, और तलाक-ए-हसन इसी सिद्धांत के निकट है।
यह सुनवाई भारतीय समाज के लिए एक सबक के रूप में सामने आई कि न्याय का मक़सद दंड नहीं, बल्कि संरक्षण और संतुलन स्थापित करना है। धार्मिक विधान चाहे जितना पुराना हो, उसका उपयोग मानव गरिमा की रक्षा के अनुरूप होना चाहिए।
क़ुरआन स्पष्ट कहता है कि महिला को मेहर, पोस्ट-डाइवोर्स मेंटेनेंस, और सम्पत्ति-स्वामित्व का अधिकार प्राप्त है। तलाक की प्रक्रिया में उसे किसी भी प्रकार से अपमानित या निष्कासित करना इस्लामी सिद्धांत के विरुद्ध है ।
हीना जैसी महिलाएँ इस न्यायिक प्रक्रिया की प्रतीक बन गई हैं, जिन्होंने अपनी आवाज़ दबने नहीं दी — और अदालत ने दिखाया कि कानून उनके साथ खड़ा है
यह फैसला केवल एक मुकदमा नहीं, बल्कि भारतीय न्यायिक इतिहास में शरिया, संवैधानिक समानता और महिला-गरिमा के बीच संतुलन का उदाहरण है। तलाक-ए-हसन पर यह निर्णय बताता है कि धर्म और कानून टकराव नहीं, बल्कि संवाद और सुधार के माध्यम बन सकते हैं।
यह केस हमें याद दिलाता है कि न्याय का वास्तविक उद्देश्य सबसे कमजोर को सबसे अधिक सुरक्षा देना है।
(लेखक निर्मल कुमार सामाजिक एवं धार्मिक मामलों के जानकार हैं।यह उनके निजी विचार हैं।)